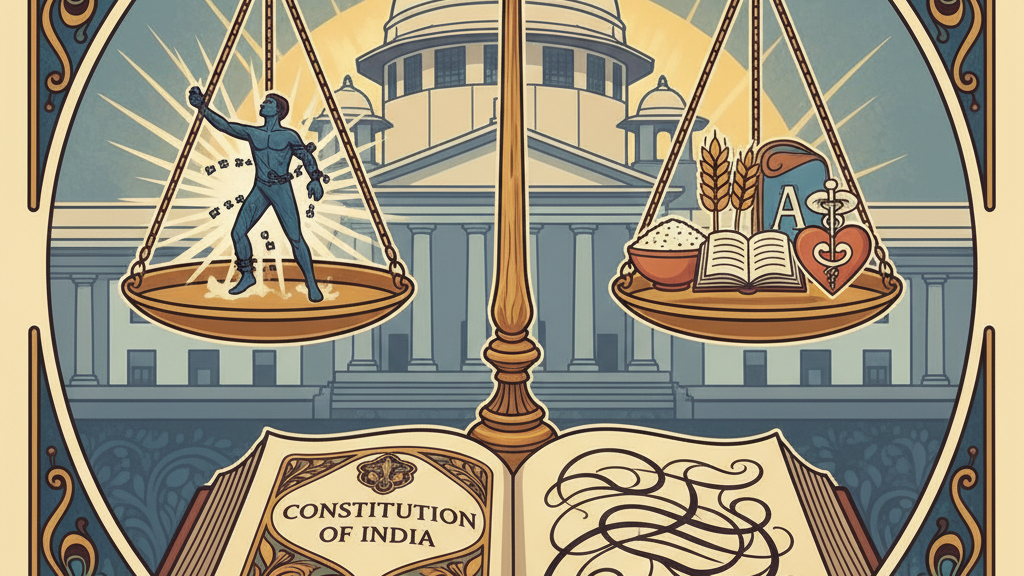
भारतीय संविधान किस प्रकार मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और स्वतंत्र न्यायपालिका के त्रिकोण के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक न्याय के बीच एक गतिशील संतुलन स्थापित करता है?
Answer: भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और स्वतंत्र न्यायपालिका की अनूठी व्यवस्था का उपयोग करता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने का मार्गदर्शन करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका इन दोनों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि नीति निर्माण में निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए, जिससे संविधान के मूलभूत मूल्यों को बनाए रखा जा सके।
भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत ग्रंथ है जो भारत के लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को साकार करने का प्रयास करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने का इसका अद्वितीय दृष्टिकोण है। यह संतुलन तीन मुख्य स्तंभों - मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार, नागरिकों को राज्य के मनमाने कृत्यों के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। ये अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता के संरक्षक हैं। ये प्रकृति में नकारात्मक हैं, अर्थात वे राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, और वे न्यायोचित (न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय) हैं। इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।वहीं, संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSPs) शामिल हैं। ये सिद्धांत राज्य के लिए आदर्श या दिशानिर्देश हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। उदाहरण के लिए, ये सिद्धांत समान काम के लिए समान वेतन, पर्याप्त आजीविका के साधन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे लक्ष्यों की दिशा में राज्य को प्रेरित करते हैं। मौलिक अधिकारों के विपरीत, ये गैर-न्याययोचित हैं, अर्थात इन्हें सीधे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि, ये देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे।इन दोनों स्तंभों के बीच संतुलन और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने में स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका न केवल मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, बल्कि वह संविधान की व्याख्या भी करती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से, न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कोई भी कानून संविधान के प्रावधानों, विशेषकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। कई ऐतिहासिक निर्णयों में, जैसे कि गोलकनाथ और केशवानंद भारती मामले में, न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या स्थापित करने का प्रयास किया है, जहाँ वह सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों को स्वीकार करती है, लेकिन उनके मूल ढांचे को अक्षुण्ण रखती है।इस प्रकार, भारतीय संविधान का यह त्रिकोण - मौलिक अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं, नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, और स्वतंत्र न्यायपालिका इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर संविधान के मूल दर्शन को अक्षुण्ण रखती है। यह व्यवस्था एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करती है जहाँ नागरिक के अधिकार सुरक्षित हों और समाज में समानता व न्याय की स्थापना हो।
Tags:
भारतीय संविधान
मौलिक अधिकार
नीति निदेशक सिद्धांत
स्वतंत्र न्यायपालिका
सामाजिक न्याय
Related Questions
- भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोकने का निर्देश देता है?
- भारतीय संविधान का कौन-सा भाग 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (Directive Principles of State Policy) से संबंधित है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है?
- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध' की गारंटी देता है?
- भारत में परिसीमन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
- निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 'अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष' के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है?
- भारत में परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
Tags
भारत की नदियाँ
जल संसाधन
नदी महत्व
भारतीय भूगोल
नदी तंत्र
प्लासी का युद्ध
रॉबर्ट क्लाइव
सिराजुद्दौला
मीर जाफ़र
ईस्ट इंडिया कंपनी
भारतीय इतिहास
1757
राष्ट्रपति
अनुच्छेद 72
क्षमादान
भारतीय संविधान
राजव्यवस्था
उपभोक्ता अधिकार
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
जागरूकता
उपभोक्ता संरक्षण
जॉन एफ. कैनेडी
संयुक्त राष्ट्र
भारत
टिकाऊ खपत
भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंक दर
मौद्रिक नीति
बैंकिंग प्रणाली
ब्याज दर
भारतीय अर्थव्यवस्था
सिंधु घाटी सभ्यता
मोहनजोदड़ो
विशाल स्नानागार
प्राचीन भारत
हड़प्पा सभ्यता
पुरातत्व
फ्रांसीसी क्रांति
क्रांति
स्वतंत्रता
समानता
बंधुत्व
लुई सोलहवें
आतंक का राज
नेपोलियन बोनापार्ट
मानवाधिकार
भारतीय सेना
सियाचिन ग्लेशियर
ऑपरेशन मेघदूत
सैन्य इतिहास
रक्षा
सचिन तेंदुलकर
टेस्ट क्रिकेट
क्रिकेट
भारतीय खिलाड़ी
रिकॉर्ड
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
योग
स्वास्थ्य
21 जून
आसन
प्राणायाम
प्राचीन यूनान
ओलंपिया के खेल
ज़्यूस
हेलेनिक सभ्यता
प्राचीन खेल
धर्म
रेगिस्तान
सहारा
अफ्रीका
भूगोल
जलवायु
वनस्पति
जीव-जंतु
इतिहास
डॉ. भीमराव अंबेडकर
संविधान सभा
मसौदा समिति
सामाजिक न्याय
गुप्त साम्राज्य
चंद्रगुप्त प्रथम
महाराजाधिराज
सम्राट अशोक
मौर्य राजवंश
कलिंग युद्ध
शिलालेख
बौद्ध धर्म
धम्म
ला टोमाटिना
स्पेन
त्योहार
उत्सव
होली
टमाटर
सांस्कृतिक
मुख्य चुनाव आयुक्त
चुनाव आयोग
भारत के राष्ट्रपति
संवैधानिक निकाय
लोकतंत्र
नियुक्ति प्रक्रिया
चुनाव
मावसिनराम
मेघालय
वर्षा
विश्व रिकॉर्ड
मानसून
नैनो प्रौद्योगिकी
सूक्ष्म विज्ञान
नैनो-सामग्री
सामग्री विज्ञान
विज्ञान और प्रौद्योगिकी
बाल अधिकार
NCPCR
बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005
किशोर न्याय अधिनियम
शिक्षा का अधिकार
बाल श्रम
बाल विवाह
वैदिक काल
गोत्र
आर्य
ऋग्वेद
उत्तरवैदिक काल
भारतीय संस्कृति
सामाजिक संरचना
पवन ऊर्जा
नवीकरणीय ऊर्जा
तमिलनाडु
ऊर्जा उत्पादन
पर्यावरण
CRISPR-Cas9
जीन संपादन
जैविक प्रौद्योगिकी
नैतिकता
मानव भ्रूण
जर्मलाइन संपादन
वैज्ञानिक अनुसंधान
नृत्यरत स्त्री
कांस्य प्रतिमा
सतत विकास
पृथ्वी शिखर सम्मेलन
जोहान्सबर्ग
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
विकास
बृहस्पति
सौरमंडल
ग्रह
हाइड्रोजन
गैसीय ग्रह
खगोल विज्ञान
अंतरिक्ष
पियानो
वाद्ययंत्र
संगीतकार
शास्त्रीय संगीत
रचना
संगीत सिद्धांत
द्वितीय विश्व युद्ध
परमाणु बम
हिरोशिमा
नागासाकी
जापान
संयुक्त राज्य अमेरिका
युद्ध का अंत
ऐतिहासिक घटनाएँ
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण
फैराडे का नियम
चुम्बकीय फ्लक्स
विद्युत वाहक बल
जनरेटर
ट्रांसफार्मर
प्रेरकत्व
मंगल
लाल ग्रह
आयरन ऑक्साइड
धन विधेयक
अनुच्छेद 110
लोकसभा
राज्यसभा
संसद
वित्तीय विधेयक
पंडित रविशंकर
सितार
भारतीय शास्त्रीय संगीत
विश्व संगीत
संगीत
जल विद्युत
भाखड़ा-नांगल
नदी
ऊर्जा
सिंचाई
परियोजना
नाटो
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन
सामूहिक रक्षा
शीत युद्ध
सैन्य गठबंधन
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा
बिग डेटा
हाडूप
डेटा विश्लेषण
ओपन-सोर्स
वितरित कंप्यूटिंग
HDFS
MapReduce
भरतनाट्यम
हस्तमुद्रा
भारतीय शास्त्रीय नृत्य
नृत्य मुद्राएँ
कला
संस्कृति
अभिनय
वैश्विक परिवार दिवस
परिवार
अंतर्राष्ट्रीय दिवस
शांति
सद्भाव
नव वर्ष
कार्बन
रसायन विज्ञान
जीवन का तत्व
कार्बनिक रसायन
कार्बन चक्र
आवर्त सारणी
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन
ISS
अंतरिक्ष अन्वेषण
NASA
Roscosmos
JAXA
CSA
ESA
अंतरिक्ष सहयोग
अंतरिक्ष विज्ञान
यूनानी सभ्यता
प्राचीन साहित्य
महाकाव्य
होमर
इलियड
ओडिसी
ग्रीक साहित्य
कृत्रिम बुद्धिमत्ता
मशीन लर्निंग
भविष्य
प्रौद्योगिकी
समाज
स्वास्थ्य सेवा
शिक्षा
कार्यबल
शासन
ऊष्मागतिकी
ऊर्जा संरक्षण
विलगित निकाय
आंतरिक ऊर्जा
भौतिकी नियम
संयुक्त राष्ट्र संघ
सुरक्षा परिषद
स्थायी सदस्य
वीटो शक्ति
अंतर्राष्ट्रीय शांति
मुख्य न्यायाधीश
CJI
सर्वोच्च न्यायालय
न्यायपालिका
संविधान
कॉलेजियम प्रणाली
गुरुत्वाकर्षण
न्यूटन
सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम
भौतिकी
बल
मानवयुक्त मिशन
यूरी गगारिन
सोवियत संघ
अंतरिक्ष दौड़
ऐतिहासिक घटना
जीनोम
डीएनए
आनुवंशिकी
बायोटेक्नोलॉजी
चिकित्सा
जलप्रपात
एंजल फॉल्स
वेनेज़ुएला
प्राकृतिक अजूबे
पर्यटन
विश्व के सबसे ऊँचे जलप्रपात
मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 24
शोषण के विरुद्ध अधिकार
कानून
बंदरगाह
वैश्विक व्यापार
माल ढुलाई
शंघाई
चीन
लॉजिस्टिक्स
अर्थव्यवस्था
समानता का अधिकार
भेदभाव का प्रतिषेध
अनुच्छेद 15
भारतीय राजव्यवस्था
मृगनयनी महल
ग्वालियर
मध्य प्रदेश
ऐतिहासिक स्थल
वास्तुकला
रानी मृगनयनी
नासा
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
अवरक्त प्रकाश
हबल स्पेस टेलीस्कोप
ब्रह्मांड
संप्रभु हरित बॉन्ड
हरित वित्त
जलवायु परिवर्तन
टिकाऊ विकास
भारत सरकार
वित्तीय साधन
सौर ऊर्जा
फोटोवोल्टेइक
अर्धचालक
ऊर्जा रूपांतरण
सकल घरेलू उत्पाद
सांकेतिक जीडीपी
वास्तविक जीडीपी
मुद्रास्फीति
आर्थिक संकेतक
परिसीमन आयोग
निर्वाचन क्षेत्र
विधानसभा
चुनाव आयुक्त
पीयूष ग्रंथि
अंतःस्रावी तंत्र
हार्मोन
मास्टर ग्रंथि
हाइपोथैलेमस
मानव शरीर
ग्रंथियाँ
विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO
विश्व स्वास्थ्य दिवस
अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य
सार्वजनिक स्वास्थ्य
ग्लोबल वार्मिंग
समुद्र तल में वृद्धि
ग्लेशियर
बर्फ की चादरें
थर्मल विस्तार
ग्रीनहाउस गैसें
नगरीय योजना
महास्नानघर
सिंधु लिपि
MSP
न्यूनतम समर्थन मूल्य
भारतीय कृषि
किसान
सरकारी नीति
खाद्य सुरक्षा
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
NLM
साक्षरता दर
कार्य कार्यात्मक साक्षरता
स्वयंसेवक
गैर-सरकारी संगठन
विश्व अर्थव्यवस्था
GDP
PPP
अमेरिका
आर्थिक विकास
आरक्षित निधि
वित्तीय नियोजन
कंपनी अधिनियम
वित्तीय स्थिरता
निवेश
ऋण प्रबंधन
सरकार
कंपनी
मौर्य साम्राज्य
चंद्रगुप्त मौर्य
अशोक
मगध
चाणक्य
अर्थशास्त्र
परमाणु विखंडन
नाभिकीय भौतिकी
परमाणु ऊर्जा
श्रृंखला अभिक्रिया
यूरेनियम
विज्ञान
सार्वत्रिक नियम
रवींद्रनाथ टैगोर
नोबेल पुरस्कार
प्रथम भारतीय
गीतांजलि
साहित्य
विश्व-भारती
आदिवासी शिक्षा
आवासीय विद्यालय
सशक्तिकरण
जनजातीय कल्याण
महासागर
प्रशांत महासागर
मारियाना ट्रेंच
चैलेंजर डीप
गहराई
विश्व
अन्वेषण
सापेक्षता का सिद्धांत
विशेष सापेक्षता
सामान्य सापेक्षता
अल्बर्ट आइंस्टीन
प्रकाश की गति
ब्रह्मांड विज्ञान
E=mc²
समय का फैलाव
लंबाई संकुचन
5G
6G
नेटवर्क
टेलीकम्युनिकेशन
तकनीक
गति
विलंबता
AI
प्रवर्तन निदेशालय
ED
मनी लॉन्ड्रिंग
PMLA
FEMA
आर्थिक अपराध
परमाणु
नाभिक
प्रोटॉन
परमाणु क्रमांक
तत्व
सैन्य अभियान
कालिदास
अभिज्ञानशाकुंतलम्
संस्कृत साहित्य
नाट्यशास्त्र
महाभारत
दुष्यंत
शकुंतला
भारतीय क्लासिक्स
रेलवे
परिवहन
लॉर्ड डलहौजी
मुंबई
ठाणे
1853
पुरस्कार
अल्पसंख्यक
सम्मान
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
प्रकाश संश्लेषण
कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन
क्लोरोफिल
जीव विज्ञान
पादप
पृथ्वी की संरचना
भूपर्पटी
मेंटल
कोर
भूविज्ञान
पृथ्वी की परतें
महाद्वीपीय भूपर्पटी
महासागरीय भूपर्पटी
संवैधानिक शक्ति
सूचना प्रौद्योगिकी
आईटी
बंगलूरु
सिलिकॉन वैली
नवाचार
उदारीकरण
हिमालय
वलित पर्वत
टेक्टोनिक प्लेटें
पर्वत श्रृंखलाएँ
नदी उद्गम
डीप लर्निंग
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क
न्यूरल नेटवर्क
तंत्रिका नेटवर्क
आसियान
दक्षिण पूर्व एशिया
अंतर्राष्ट्रीय संगठन
हरित बॉन्ड
पर्यावरण वित्तपोषण
रोमन साम्राज्य
पैनथिऑन
प्राचीन वास्तुकला
रोम
गुंबद
हैड्रियन
इंजीनियरिंग
सोफिया
रोबोटिक्स
हैनसन रोबोटिक्स
ह्यूमनॉइड रोबोट
P5
अंतर्राष्ट्रीय कानून
भू-राजनीति
जनसंख्या
प्रतिनिधित्व
फिनलैंड
झीलें
नॉर्डिक देश
राजधानियाँ
प्रधानमंत्री
जयपुर
गुलाबी शहर
राजस्थान
विश्व धरोहर स्थल
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
NHM
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
NUHM
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
NRHM
स्वास्थ्य सेवाएँ
जन स्वास्थ्य
अटलांटिक की लड़ाई
काफिला प्रणाली
पनडुब्बी युद्ध
मित्र राष्ट्र
धुरी राष्ट्र
नौसेना
रणनीति
आयरन
लौह
हीमोग्लोबिन
रक्त
शरीर विज्ञान
खनिज
पोषण
विश्व के देश
क्षेत्रफल
वेटिकन सिटी
रूस
सबसे छोटा देश
सबसे बड़ा देश
ओपन ऑफर
शेयर बाजार
अधिग्रहण
SEBI
कॉर्पोरेट गवर्नेंस
भोजन की बर्बादी
खाद्य अपव्यय
उपभोक्ता व्यवहार
संसाधन प्रबंधन
कृषि
चोल राजवंश
दक्षिण भारत
राजेंद्र प्रथम
राजराज प्रथम
साम्राज्य
वर्ल्ड वाइड वेब
टिम बर्नर्स-ली
CERN
HTML
HTTP
URL
इंटरनेट
आविष्कार
प्लाज्मा
पदार्थ की अवस्थाएँ
आयन
इलेक्ट्रॉन
सूर्य
संलयन
जैव विविधता
पश्चिमी घाट
हॉटस्पॉट
पारिस्थितिकी तंत्र
वन्यजीव
संरक्षण
बागवानी
भारतीय परंपरा
टिकाऊ खेती
जैव-विविधता
पंच-पल्लव
प्राकृतिक संसाधन
उपग्रह
भूस्थैतिक कक्षा
GEO
संचार
रॉकेट
कक्षीय यांत्रिकी
विराट कोहली
ODI क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट
क्रिकेटर
खेल
यूरेनियम-235
नाभिकीय विखंडन
समस्थानिक
ऊर्जा स्रोत
पोलिस
नगर-राज्य
एथेंस
स्पार्टा
अमर्त्य सेन
भारतीय विजेता
कल्याणकारी अर्थशास्त्र
नोबेल लॉरिएट
विकास अर्थशास्त्र
ग्रीनहाउस प्रभाव
प्रदूषण
DRDO
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
IGMDP
पृथ्वी मिसाइल
मिसाइल मैन
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत की रक्षा
आत्मनिर्भर भारत
खाड़ियाँ
मेक्सिको की खाड़ी
बंगाल की खाड़ी
फ़ारसी खाड़ी
हडसन खाड़ी
समुद्री भूगोल
विश्व भूगोल
जलीय निकाय
जूट
सुनहरा रेशा
फसल उत्पादन
फाइबर
नकदी फसल
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
चार्टर
सैन फ्रांसिस्को
महासचिव
जीन एडिटिंग
जैव प्रौद्योगिकी
वैज्ञानिक खोज
भारत के मुख्य न्यायाधीश
सेवानिवृत्ति आयु
रोस्टर का मास्टर
मृदा विज्ञान
काली मिट्टी
रेगुर मिट्टी
मिट्टी के प्रकार
भारत का भूगोल
दक्कन का पठार
कपास
विधायिका
हाइड्रोपोनिक्स
मिट्टी रहित खेती
शहरी खेती
भविष्य की कृषि
भारतीय मुद्रा
सिक्के
रुपया
शेरशाह सूरी
मध्यकालीन भारत
ब्रिटिश राज
स्वतंत्रता के बाद मुद्रा
किले
महल
आमेर किला
राजपूत
मुगल
विरासत
राजा मान सिंह प्रथम
राज्य के नीति निदेशक तत्व
DPSP
भाग IV
कल्याणकारी राज्य
भारत का शासन
वेद
अथर्ववेद
सामवेद
यजुर्वेद
कॉस्मिक किरणें
विक्टर हेस
खगोल भौतिकी
कण भौतिकी
सुपरनोवा
विकिरण
भूस्खलन
बृहत् संचलन
विसर्पण
प्राकृतिक आपदा
मिट्टी का कटाव
ढलान स्थिरता
ओजोन परत
विश्व ओजोन दिवस
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
UNEP
UV विकिरण
समताप मंडल
रिवर्स रेपो दर
तरलता प्रबंधन
मुद्रास्फीति नियंत्रण
आर्थिक नीति
बैंकिंग
जीनोम अनुक्रमण
मानव जीनोम परियोजना
व्यक्तिगत चिकित्सा
NGS
अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति
G20
G7
शिखर सम्मेलन
शेरपा
बहुपक्षीय मंच
वैश्विक शासन
संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
CBD
पारिस्थितिकी
अंतर्राष्ट्रीय समझौते
प्राचीन विश्व
आधुनिक विश्व
स्मारक
मानव निर्मित चमत्कार
मिस्र
विलय और अधिग्रहण
कॉर्पोरेट लेनदेन
वित्तीय बाजार
ज्ञानपीठ पुरस्कार
आशापूर्णा देवी
बंगाली साहित्य
महिला साहित्यकार
भारतीय साहित्य
उपन्यासकार
प्रथम प्रतिश्रुति
दूरसंचार
वायरलेस तकनीक
इंटरनेट ऑफ थिंग्स
बैंडविड्थ
IoT
स्मार्ट टेक्नोलॉजी
कनेक्टेड डिवाइस
डेटा
ऑटोमेशन
डिजिटल परिवर्तन
एन्ट्रॉपी
ऊष्मागतिकी के नियम
परमाणु रिएक्टर
नियंत्रण छड़ें
न्यूट्रॉन
सुरक्षा
स्वच्छ ऊर्जा
धोलावीरा
जल प्रबंधन
पुरातात्विक स्थल
यूनेस्को
वित्तीय अपराध
भारत का कानून
अधिनियम
राजवंश
श्रीगुप्त
स्वर्ण युग
समुद्रगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय
सेंसर
कनेक्टिविटी
उद्योग 4.0
एआई
स्मार्ट होम
स्मार्ट सिटीज़
व्यपगत का सिद्धांत
भारत का इतिहास
1857 का विद्रोह
रियासतें
साम्राज्यवादी नीति
विलय नीति
ऑस्कर
अकादमी पुरस्कार
विंग्स
हॉलीवुड
विश्व सिनेमा
मूक फिल्म
सिनेमा इतिहास
प्रथम विश्व युद्ध
विलियम ए. वेलमैन
भारत रत्न
नागरिक सम्मान
खान अब्दुल गफ्फार खान
सीमांत गांधी
राष्ट्रीय पुरस्कार
भारतीय वास्तुकला
सांस्कृतिक विरासत
यूनेस्को विश्व धरोहर
राष्ट्रीय प्रतीक
राष्ट्रीय ध्वज
अशोक स्तंभ
राष्ट्रीय गान
भारतीय त्योहार
धार्मिक महत्व
कृषि पर्व
सामाजिक एकता
लोक नृत्य
राज्यवार नृत्य
भारतीय कला
भारत पर्यटन
हिमालयी पर्यटन
प्राकृतिक सौंदर्य
तीर्थस्थल
साहसिक पर्यटन
चट्टानें
आग्नेय चट्टानें
अवसादी चट्टानें
रूपांतरित चट्टानें
पृथ्वी
भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ
चट्टान चक्र
प्रधान मंत्री
संसदीय प्रणाली
अनुच्छेद 75
कार्यपालिका
परिशुद्ध कृषि
स्मार्ट फार्मिंग
कृषि नवाचार
किसानों की आय
जल संरक्षण
उर्वरक प्रबंधन
डेटा-संचालित कृषि
गौतम बुद्ध
सिद्धार्थ
विश्व धर्म
दर्शन
निर्वाण
अष्टांगिक मार्ग
चार आर्य सत्य
भारत की पहचान
एकता और विविधता
संवैधानिक आदर्श
राजस्थान पर्यटन
ऐतिहासिक स्मारक
अतीत का महत्व
भारतीय पर्यटन
स्थानीय अर्थव्यवस्था
विरासत संरक्षण
इसरो
अंतरिक्ष कार्यक्रम
आत्मनिर्भरता
सामाजिक विकास
परंपराएँ
अध्यात्म
सामाजिक सद्भाव
प्रकृति
अशोक चक्र
सारनाथ स्तंभ
भारतीय प्रतीक
तिरंगा
मूल्य
एकता
पहचान
सत्यमेव जयते
नीति निदेशक सिद्धांत
स्वतंत्र न्यायपालिका
कंचनजंघा
पुरस्कार विजेता
भारतीय रेल
विद्युतीकरण
फ्रेट कॉरिडोर
आधुनिकीकरण
स्थायी विकास
चंद्रयान-3
चंद्रमा
सॉफ्ट लैंडिंग
गौरव
लाल किला
मुगल वास्तुकला
दिल्ली
मंगलयान
मंगल मिशन
PSLV
भारतीय रेलवे
वंदे भारत
समर्पित माल ढुलाई गलियारा
भारतीय पहचान
जन गण मन
विश्व धरोहर
भारतीय विरासत
एएसआई
भारतीय नदियाँ
गंगा नदी
नदी संरक्षण
राष्ट्रीय पहचान
गणतंत्र दिवस
पूर्ण स्वराज
राष्ट्रीय पर्व
धार्मिक पर्व
भारत की संस्कृति
प्राचीन स्मारक
सांस्कृतिक धरोहर
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक
राष्ट्रीय एकता
प्रतीकात्मक महत्व
भारत के दिवस
सामाजिक जागरूकता
ऐतिहासिक स्मरण
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
सांस्कृतिक स्थल
प्राकृतिक स्थल
स्थापत्य कला
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम
चंद्रयान
प्रक्षेपण यान
सांस्कृतिक महत्व
विविधता
सामाजिक सौहार्द
विश्व विरासत
सांस्कृतिक संरक्षण
भारत छोड़ो आंदोलन
महात्मा गांधी
स्वतंत्रता संग्राम
7 अप्रैल
वित्तीय प्रबंधन
संसदीय प्रक्रिया
भौतिक विज्ञान
क्वांटम यांत्रिकी
अनिश्चितता सिद्धांत
वर्नर हाइजेनबर्ग
क्वांटम भौतिकी
अस्तित्ववाद
जीन-पॉल सार्त्र
अल्बर्ट कैमुस
सिमोने द बोवोयर
दर्शनशास्त्र
20वीं सदी का दर्शन
WWW
वेब विकास
जोहान सेबेस्टियन बाख
बैरोक संगीत
कीबोर्ड यंत्र
ऑर्गन
हार्पसीकोर्ड
संगीत का इतिहास
अनुच्छेद 370
जम्मू और कश्मीर
राजनीति
विशेष दर्जा
5 अगस्त 2019
साइबर सुरक्षा
फ़िशिंग
सुरक्षा उपाय
डेटा सुरक्षा
ऑनलाइन सुरक्षा
नियुक्ति
ARPANET
कंप्यूटर
नेटवर्किंग
टेक्नोलॉजी
सापेक्षता
आइंस्टाइन
वैज्ञानिक सिद्धांत
विज्ञान के सिद्धांत
महासभा
विश्व शांति
इलेक्ट्रिक वाहन
सरकारी नीतियाँ
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस
प्रेस स्वतंत्रता
पत्रकारिता
मीडिया
स्वास्थ्य नीति
नदियाँ
नील नदी
अमेज़ॅन नदी
यांग्त्ज़े नदी
मिसिसिपी नदी
युद्ध
मुगल साम्राज्य
ब्रिटिश साम्राज्य
सैन्य योगदान
भारतीय भाषाएँ
भाषा-परिवार
भाषा-समूह
जानवर
स्तनधारी
चुनौतियाँ
योजना आयोग
नीति आयोग
राजनीतिक अर्थव्यवस्था
अधिकार
प्रस्तावना
गणराज्य
आदर्श
शहर
आकार
मत्स्य पालन
जल प्रदूषण
लुप्तप्राय प्रजातियाँ
वन्यजीव संरक्षण
असमानता
नीति
हीनयान
महायान
संप्रदाय
गांधीजी
अहिंसा
सत्याग्रह
भौगोलिक विविधता
मरुस्थल
तट
जलग्रहण क्षेत्र
मैदान
भौतिक भूगोल
गंगा मैदान
थार रेगिस्तान
तटरेखा
भू-आकृतियाँ
CFCs
पर्यावरण प्रदूषण
पराबैंगनी विकिरण
स्टेम सेल
थेरेपी
भ्रूणीय स्टेम सेल
वयस्क स्टेम सेल
प्लास्टिसिटी
हड़प्पा
हरित क्रांति
उर्वरक
यूरिया
तकनीकी
टर्बाइन
बैटरी
ऊर्जा भंडारण
लिथियम-आयन
लीड-एसिड