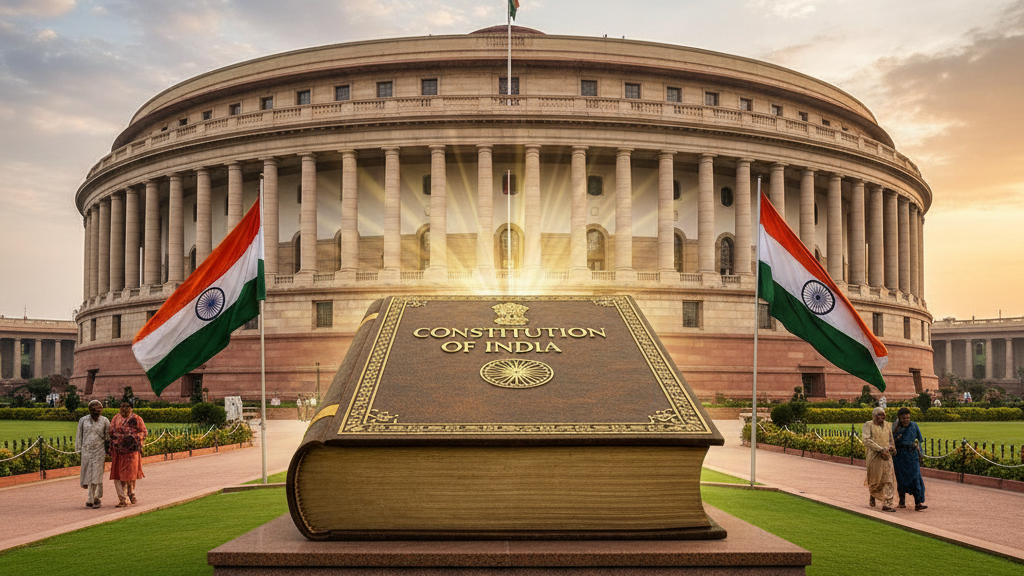
भारतीय संविधान का कौन-सा भाग 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (Directive Principles of State Policy) से संबंधित है?
Answer: भाग IV
भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, और इसके नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व सुनिश्चित करता है। यह राष्ट्र की सर्वोच्च विधि है, जो सरकार के विभिन्न अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—के कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करती है, साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट करती है।
इस विशाल दस्तावेज़ का निर्माण भारत की संविधान सभा ने लगभग तीन वर्षों (2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन) में पूरा किया। संविधान निर्माताओं ने दुनिया के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रावधानों को अपनाया, जिससे एक अद्वितीय दस्तावेज़ का जन्म हुआ। उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण एक ऐसे भारत की कल्पना करता था जहाँ प्रत्येक नागरिक को गरिमा और अवसर मिले, और राष्ट्र की विविधता को समायोजित किया जा सके।
भारतीय संविधान अपनी कई विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें इसका विशाल आकार, विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, तथा एक संघीय प्रणाली शामिल है जिसमें एक मजबूत केंद्र का झुकाव है। इसकी प्रस्तावना, जिसे अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसके मूल दर्शन और आदर्शों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। यह 'हम भारत के लोग' शब्दों से शुरू होती है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान उद्देश्यों को घोषित करती है।
संविधान के 'भाग III' में निहित मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के मनमाने कृत्यों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार न्यायोचित (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि इनके उल्लंघन पर नागरिक सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं। ये व्यक्ति की गरिमा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के स्तंभ हैं।
मौलिक अधिकार जहाँ व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित हैं, वहीं संविधान का 'भाग IV' राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy – DPSP) से संबंधित है। ये तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य को दिशानिर्देश प्रदान करते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये मौलिक अधिकारों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ मौलिक अधिकार 'क्या नहीं करना चाहिए' बताते हैं, वहीं DPSP 'क्या करना चाहिए' का मार्गदर्शन करते हैं।
राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जहाँ इन्हें 'सामाजिक नीति के निदेशक सिद्धांत' कहा जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन सिद्धांतों को इस विश्वास के साथ अपनाया कि भविष्य की सरकारें इन आदर्शों के अनुरूप अपनी नीतियां बनाएंगी। इनका उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना ही नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था, जहाँ समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित हो।
DPSP की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये 'गैर-न्यायोचित' (non-justiciable) हैं। इसका अर्थ है कि यदि राज्य इन सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहता है, तो नागरिक इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में राज्य का कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे। वे राज्य के लिए नैतिक और संवैधानिक दायित्व का प्रतीक हैं।
नीति निदेशक तत्वों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनमें अनुच्छेद 38 (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना), अनुच्छेद 39 (सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण रोकना, समान काम के लिए समान वेतन), अनुच्छेद 41 (बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 43A (उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी) जैसे प्रावधान शामिल हैं।
गांधीवादी सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित हैं, जो ग्रामीण विकास और ग्राम स्वराज की अवधारणा पर जोर देते हैं। इनमें अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतों का संगठन), अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना), अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना), अनुच्छेद 47 (पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार) और अनुच्छेद 48 (कृषि और पशुपालन का संगठन, विशेषकर गोहत्या पर प्रतिबंध) शामिल हैं।
उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत व्यक्तिवाद और सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित हैं। इनमें अनुच्छेद 44 (नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता), अनुच्छेद 45 (सभी बच्चों के लिए छह साल की उम्र पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना), अनुच्छेद 48A (पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा), अनुच्छेद 49 (राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण), अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण) और अनुच्छेद 51 (अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना) शामिल हैं।
DPSP भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ हैं। यद्यपि ये कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी ये सरकारों के लिए एक नैतिक और नीतिगत मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। ये एक ऐसे भारत का खाका प्रस्तुत करते हैं जहाँ गरीबी, असमानता और अशिक्षा समाप्त हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई निर्णयों में DPSP को मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए व्याख्यायित किया है, जिससे इनके महत्व को और बल मिला है।
मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संबंध भारतीय संवैधानिक कानून के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक रहा है। केशवानंद भारती मामले (1973) और मिनर्वा मिल्स मामले (1980) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने यह स्थापित किया कि मौलिक अधिकार और DPSP एक-दूसरे के पूरक हैं और संविधान के सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। न्यायालय ने 'संविधान के मूल ढांचे' की अवधारणा को पेश करते हुए इनके बीच सामंजस्य पर जोर दिया।
कई संवैधानिक संशोधनों ने DPSP के दायरे और महत्व को बढ़ाया है। 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने कुछ नए DPSP जोड़े, जैसे अनुच्छेद 39A (गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता), अनुच्छेद 43A (उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी), और अनुच्छेद 48A (पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा)। भारत में कई कानून और नीतियां DPSP को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जैसे पंचायती राज प्रणाली (अनुच्छेद 40), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (अनुच्छेद 45), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम (अनुच्छेद 42) आदि।
DPSP की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि वे गैर-न्यायोचित होने के कारण केवल 'नैतिक उपदेश' बनकर रह जाते हैं, जिन्हें सरकारें अपनी सुविधानुसार लागू करती हैं या अनदेखा करती हैं। इनकी अस्पष्टता और संसाधनों की कमी भी इनके पूर्ण कार्यान्वयन में बाधा डालती है। हालांकि, ये सरकार पर एक निरंतर दबाव बनाए रखते हैं कि वह सामाजिक-आर्थिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करे, और ये शासन के लिए एक आवश्यक दिशा-निर्देशक बने रहते हैं।
संक्षेप में, भारतीय संविधान का भाग IV, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से, भारत को एक वास्तविक अर्थों में कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक और नीतिगत कंपास के रूप में कार्य करते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। आज के बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में, क्या DPSP की प्रासंगिकता और उनका न्यायिक प्रवर्तन बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वे केवल आदर्श न रहकर वास्तविकता बन सकें?
Related Questions
- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोकने का निर्देश देता है?
- भारतीय संविधान किस प्रकार मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और स्वतंत्र न्यायपालिका के त्रिकोण के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक न्याय के बीच एक गतिशील संतुलन स्थापित करता है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है?
- भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है?
- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध' की गारंटी देता है?
- भारत में परिसीमन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है?
- भारत में परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है?