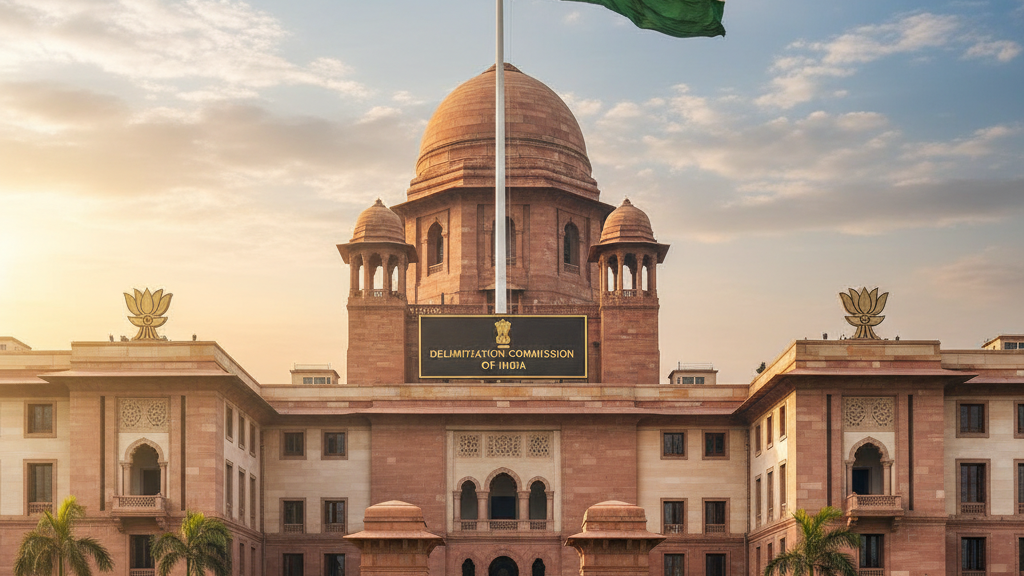
भारत में परिसीमन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
Answer: भारत में परिसीमन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
भारत में परिसीमन आयोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य कार्य देश की लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना है। यह प्रक्रिया जनसंख्या के आंकड़े, भौगोलिक सीमाओं और जनसांख्यिकीय बदलावों के आधार पर की जाती है। परिसीमन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या यथासंभव समान हो, जिससे 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत का पालन हो सके और चुनावी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और न्यायसंगत बन सके।
परिसीमन आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत की गई है। यह अनुच्छेद कहता है कि परिसीमन अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: समायोजन किया जाएगा। हालाँकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस तरह का पुन: समायोजन 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आकड़ों के आधार पर ही किया जाएगा। लेकिन, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाता है, जब तक कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि अन्यथा प्रावधान न करे।
परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस आयोग में आमतौर पर पदेन सदस्य (Ex-officio members) और पूर्णकालिक सदस्य (Full-time members) होते हैं। पदेन सदस्यों में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner of India) और संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त (State Election Commissioners) शामिल होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य, जो अक्सर सेवानिवृत्त न्यायाधीश या प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इन सदस्यों का चयन निष्पक्षता और विशेषज्ञता को ध्यान में रखकर किया जाता है।
परिसीमन आयोग का कार्य अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण होता है। यह न केवल जनसंख्या घनत्व बल्कि भौगोलिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं और मतदाताओं की सुविधा जैसे कारकों को भी ध्यान में रखता है। आयोग विभिन्न हितधारकों, जैसे कि राजनीतिक दलों, जन प्रतिनिधियों और आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करता है। इन सुझावों और आपत्तियों पर विचार-विमर्श करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना आयोग का परम कर्तव्य होता है।
अब तक भारत में चार बार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है। पहला परिसीमन 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 में हुआ था। 1976 में, संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से, 2000 तक परिसीमन को स्थगित कर दिया गया था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा सके। बाद में, 84वें संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
परिसीमन प्रक्रिया में दो मुख्य चरण होते हैं: पहला, संसद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना और दूसरा, राज्यों के विधानमंडलों के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना। संसद और विधानमंडलों के पास इन प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होता है, लेकिन वे उन्हें संशोधित नहीं कर सकते। यदि दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह कानून बन जाता है।
परिसीमन आयोग के निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह इसे एक अत्यंत शक्तिशाली और अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था बनाता है। इस शक्ति के साथ भारी जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि आयोग के निर्णय देश की राजनीतिक संरचना और प्रतिनिधित्व को प्रभावित करते हैं।
परिसीमन की आवश्यकता समय-समय पर महसूस की जाती है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और लोगों के पलायन के कारण निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या में असमानता आ जाती है। इस असमानता को दूर करने और सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन एक आवश्यक प्रक्रिया है।
हाल के वर्षों में, परिसीमन आयोग की भूमिका और उसके द्वारा लिए गए निर्णयों पर काफी बहस और चर्चा हुई है। विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने के बाद, वहां परिसीमन का कार्य पहली बार किया गया, जिसने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। इसी तरह, पूर्वोत्तर राज्यों में भी परिसीमन की मांगें उठती रही हैं।
यह प्रक्रिया भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की बदलती जनसांख्यिकी को प्रतिबिंबित करते हुए, सभी नागरिकों का उचित प्रतिनिधित्व हो। इस प्रकार, परिसीमन आयोग की नियुक्ति और उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका भारतीय लोकतंत्र की अखंडता और निष्पक्षता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि परिसीमन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को और बढ़ाया जाना चाहिए?
Related Questions
- भारत में परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है?
- भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है?
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, धन विधेयक किसे कहा जाता है और इसके क्या लक्षण हैं?
- भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोकने का निर्देश देता है?