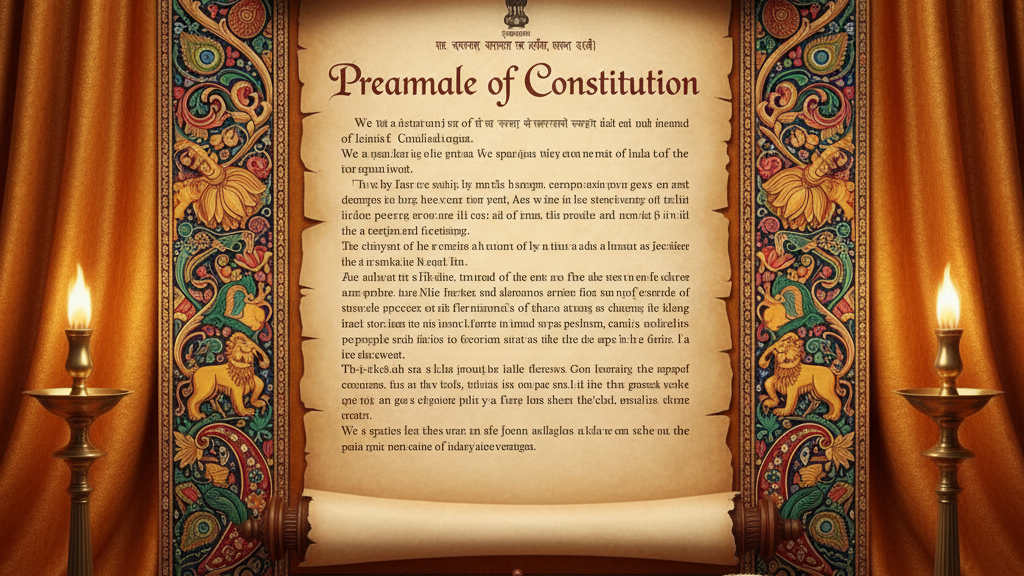
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोकने का निर्देश देता है?
Answer: अनुच्छेद 24
भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधान है। यह देश की राजनीतिक प्रणाली, मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और सरकारी निकायों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने का प्रयास किया जो सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित हो। इस महान दस्तावेज के निर्माण में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है।
भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू मौलिक अधिकार हैं, जो नागरिकों को राज्य की मनमानी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के निर्माण में भी योगदान देते हैं।
शोषण के विरुद्ध अधिकार, विशेष रूप से, समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर केंद्रित है। इस अधिकार के अंतर्गत दो प्रमुख अनुच्छेद हैं: अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बेगार को प्रतिबंधित करता है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को जबरन काम पर नहीं लगाया जा सकता और न ही उनका खरीद-बिक्री की जा सकती है। यह अनुच्छेद प्राचीन काल से चली आ रही दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करता है।
अनुच्छेद 24, जिसका प्रश्न में उल्लेख किया गया है, बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य बच्चों के नाजुक बचपन और उनके शारीरिक व मानसिक विकास की सुरक्षा करना है। यह मानता है कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने और खेलने का अधिकार है, न कि खतरनाक परिस्थितियों में काम करने का।
बाल श्रम एक वैश्विक समस्या रही है, और भारत ने इस समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। संविधान का अनुच्छेद 24 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने कानूनी ढांचा प्रदान किया जिसके तहत बाल श्रम को प्रतिबंधित किया जा सके। इसके अलावा, समय के साथ, भारत सरकार ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 जैसे विभिन्न कानून भी बनाए हैं, जो अनुच्छेद 24 के प्रावधानों को और अधिक मजबूत करते हैं। ये कानून विभिन्न आयु समूहों के बच्चों के लिए काम करने की विशिष्ट परिस्थितियों और निषेधों को परिभाषित करते हैं।
हालांकि, अनुच्छेद 24 केवल एक निषेधात्मक प्रावधान नहीं है, बल्कि यह राज्य पर एक सकारात्मक जिम्मेदारी भी डालता है। यह अनुच्छेद राज्य को उन नीतियों को बनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करता है जो बाल श्रम की जड़ों को खत्म करने में मदद करें। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक जागरूकता की कमी बाल श्रम के प्रमुख कारण हैं। इसलिए, राज्य को शिक्षा के प्रसार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसी पहलों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
भारत में बाल श्रम की समस्या जटिल और बहुआयामी है। यह अक्सर आर्थिक मजबूरी से उत्पन्न होती है, जहां परिवारों को जीवित रहने के लिए अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शिक्षा तक पहुंच की कमी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव भी इस समस्या को बढ़ाता है। इसके अलावा, कुछ पारंपरिक व्यवसायों और उद्योगों में बाल श्रम का प्रचलन आज भी देखा जाता है, जो समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है।
अनुच्छेद 24 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मजबूत प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है। सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नागरिक समाज को मिलकर बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करना होगा। बच्चों की पहचान, उन्हें बाल श्रम से मुक्त कराना, पुनर्वास और उन्हें शिक्षा प्रदान करना इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण हैं। बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें बाल श्रम के खतरों के बारे में शिक्षित करना भी आवश्यक है।
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy - DPSP) भी अप्रत्यक्ष रूप से बाल अधिकारों की सुरक्षा में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 39 (f) में कहा गया है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमा के वातावरण में स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर मिलें और बचपन और युवावस्था को शोषण से बचाया जाए। यह सिद्धांत अनुच्छेद 24 के प्रावधानों को पूरक बनाता है और एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कई संधियाँ और घोषणाएँ हुई हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (UNCRC) प्रमुख है। भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। भारतीय संविधान के प्रावधान UNCRC के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जो बाल श्रम के उन्मूलन और बच्चों के समग्र विकास पर जोर देते हैं।
कानूनी प्रावधानों के बावजूद, बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन एक लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। शिक्षा को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाकर, परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके, और बाल श्रम के खिलाफ सामाजिक जागरूकता बढ़ाकर ही हम अनुच्छेद 24 के वास्तविक सार को प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक दायित्व है कि हर बच्चा सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षा से भरपूर बचपन का आनंद ले सके।
क्या अनुच्छेद 24 केवल एक कानूनी प्रतिबंध है, या यह एक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक मार्गदर्शक सिद्धांत भी है?
Related Questions
- भारतीय संविधान का कौन-सा भाग 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (Directive Principles of State Policy) से संबंधित है?
- भारतीय संविधान किस प्रकार मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और स्वतंत्र न्यायपालिका के त्रिकोण के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक न्याय के बीच एक गतिशील संतुलन स्थापित करता है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है?
- भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
- भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया है, और यह किस अधिनियम के तहत कार्य करता है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है?
- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध' की गारंटी देता है?
- भारत में परिसीमन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है?
- भारत में परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?