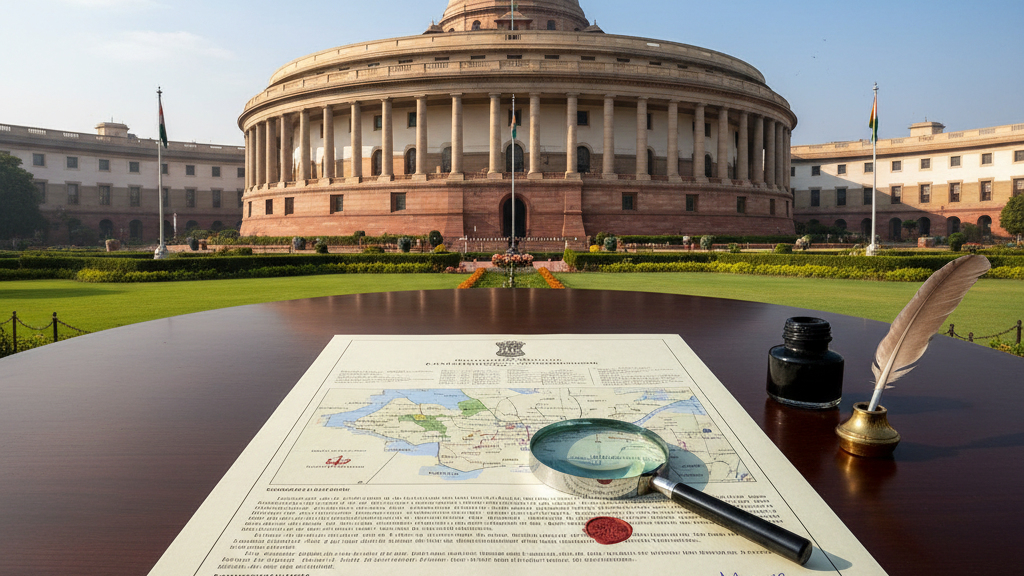
भारत में परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
Answer: भारत में परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के परिसीमन (पुनर्निर्धारण) के लिए आधार प्रदान करना है, ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग समान हो।
भारत में, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करती है। यह प्रक्रिया 'परिसीमन आयोग' नामक एक निकाय द्वारा की जाती है। परिसीमन आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद, संसद एक परिसीमन अधिनियम पारित करती है, जिसके आधार पर परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का इस प्रकार पुन: निर्धारण करना है कि देश में सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या में यथासंभव समानता बनी रहे।
परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो पूरी तरह से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से काम करता है। आयोग के सदस्यों में एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अध्यक्ष के रूप में), मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। आयोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न आंकड़ों, जैसे जनगणना के आंकड़ों, का उपयोग करता है। यह आयोग केवल जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुन: निर्धारण ही नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि भौगोलिक क्षेत्र, संचार की सुविधा और एक क्षेत्र की प्राकृतिक सीमाओं जैसी बातों का भी ध्यान रखा जाए।
परिसीमन की प्रक्रिया का इतिहास स्वतंत्रता-पूर्व काल से जुड़ा हुआ है। भारत के स्वतंत्रता के बाद, पहला परिसीमन 1952 में हुआ। इसके बाद 1961, 1971 की जनगणनाओं के आधार पर परिसीमन आयोगों का गठन किया गया। हालांकि, 1976 में, संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से, परिसीमन को 2001 की जनगणना तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसका मुख्य कारण जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देना था। बाद में, 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की आवश्यकता महसूस हुई और 2002 में परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत एक बार फिर परिसीमन आयोग का गठन किया गया।
परिसीमन आयोग के गठन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में हर नागरिक का वोट समान मूल्य रखे। यदि निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या में भारी असमानता होती है, तो कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व दूसरों की तुलना में अधिक या कम हो जाता है, जो 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य' के सिद्धांत का उल्लंघन है। परिसीमन आयोग इस असमानता को दूर करने का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकें।
आयोग की कार्यप्रणाली में विभिन्न चरणों को शामिल किया गया है। सबसे पहले, आयोग संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और भारत के महापंजीयक से आवश्यक डेटा प्राप्त करता है। इसके बाद, आयोग प्रस्तावित परिसीमन का मसौदा तैयार करता है और इसे सार्वजनिक डोमेन में रखता है ताकि जनता की आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें। विभिन्न हितधारकों, जैसे राजनीतिक दलों, स्थानीय नेताओं और आम नागरिकों को अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाता है। इन सुझावों और आपत्तियों पर विचार-विमर्श करने के बाद, आयोग अंतिम परिसीमन आदेश जारी करता है।
परिसीमन आयोग की भूमिका केवल सीटों की संख्या का पुन: निर्धारण करने तक ही सीमित नहीं है। यह अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी करता है। यह आरक्षण जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, ताकि इन समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। परिसीमन आदेशों को सीधे लागू किया जाता है और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि, आयोग के कामकाज की प्रक्रिया की निगरानी संसद कर सकती है।
हाल के वर्षों में, भारत में परिसीमन की प्रक्रिया ने विशेष रूप से कुछ राज्यों में महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। कुछ राज्यों का तर्क है कि उनकी जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद, उन्हें प्रतिनिधित्व में वृद्धि नहीं मिली है, जबकि अन्य राज्यों का कहना है कि उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है। परिसीमन आयोग का कार्य इन जटिल मुद्दों को हल करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिनिधित्व पूरी तरह से जनसंख्या के आधार पर, निष्पक्ष और समान हो।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिसीमन आयोग का गठन केवल तभी किया जाता है जब सरकार द्वारा इसके लिए कानून बनाया जाता है। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संवैधानिक और विधायी प्रावधानों के तहत की जाने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया है। आयोग द्वारा जारी किए गए अंतिम आदेश अगले परिसीमन तक प्रभावी रहते हैं। भारत के संघीय ढांचे में, परिसीमन की प्रक्रिया राज्यों और केंद्र के बीच प्रतिनिधित्व के संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त होने के कारण, वहाँ भी परिसीमन की प्रक्रिया हुई है, जिसने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया है। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में भी परिसीमन का कार्य संपन्न हुआ है, जिसका वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन क्षेत्रों में, परिसीमन की प्रक्रिया न केवल प्रतिनिधित्व बल्कि क्षेत्रीय अखंडता और जातीय समुदायों के हितों को भी प्रभावित करती है।
परिसीमन आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता को बनाए रखना देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक शक्ति का वितरण आबादी के आधार पर हो, न कि किसी अन्य कारक के आधार पर। यह प्रक्रिया समय-समय पर आयोजित की जाती है ताकि बदलती जनसंख्या के अनुसार चुनावी नक्शा अद्यतन रहे। क्या यह कभी संभव है कि परिसीमन में जनसंख्या के अलावा अन्य कारकों जैसे भौगोलिक आकार, आर्थिक महत्व, या सांस्कृतिक एकरूपता को भी समान रूप से महत्व दिया जाए?
Related Questions
- भारत में परिसीमन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है?
- भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, धन विधेयक किसे कहा जाता है और इसके क्या लक्षण हैं?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है?
- भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोकने का निर्देश देता है?
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है?
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है?